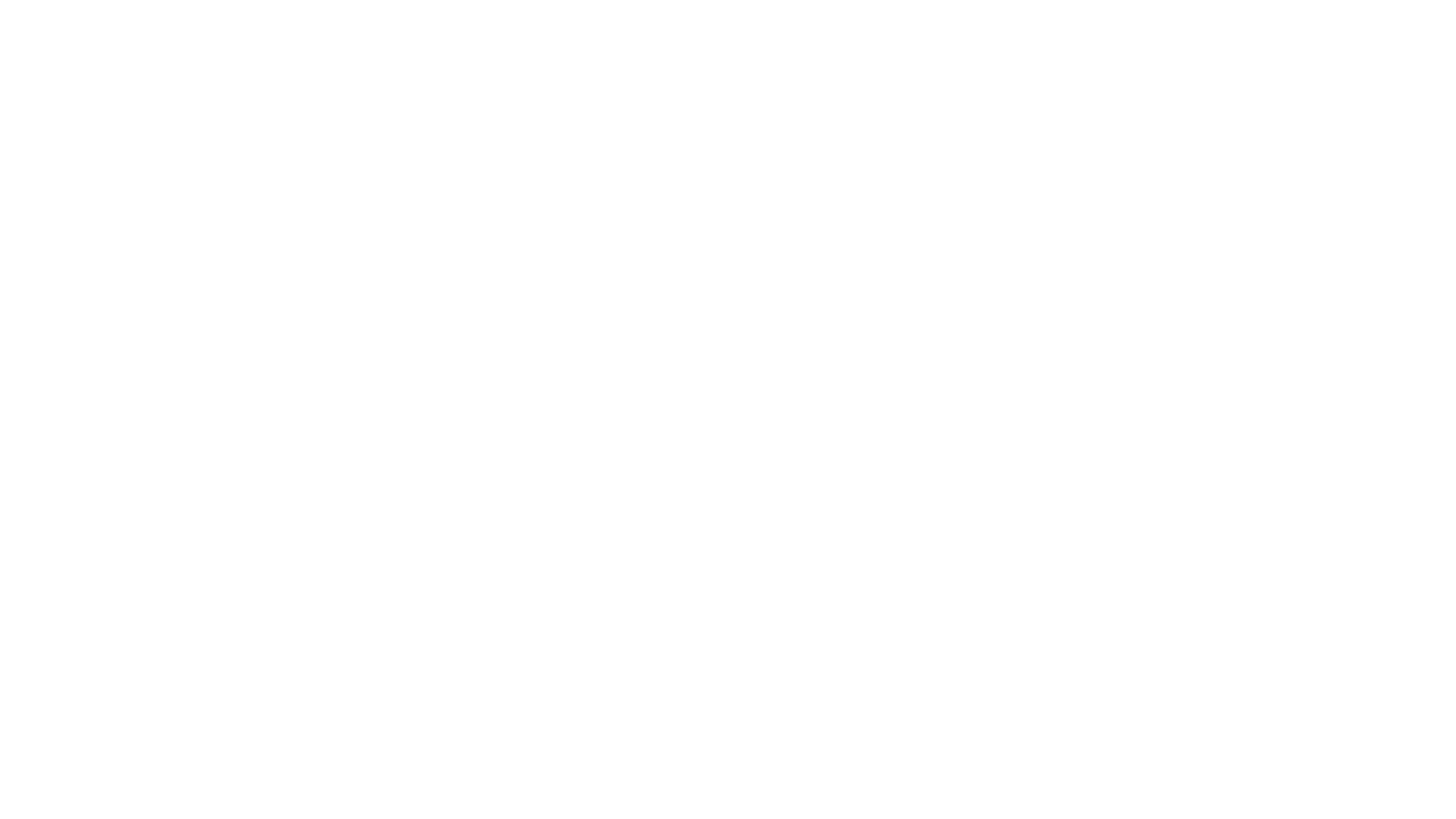आलेख
आज के युग में पूजा की प्राणवस्तु अर्थात आध्यात्म साधना तिरोहित होने लगी है और जिन देवी-देवताओं की सत्यप्रतिष्ठा, प्राणप्रतिष्ठा एवं आनन्दप्रतिष्ठा होना चाहिये हम सत्य और आनन्द की प्रतिष्ठा किये बिना सिर्फ मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा कर साधना करते है वह बाहरी आडम्बर और तामसिक उत्सव अनुष्ठानों का रूप ले चुकी है। जो भी जीवन्त आध्यात्म साधना रही है उसका प्रतिपादन वैदिक पद्धति ने किया ताकि इस आध्यात्म साधना की अविरत धारा में जो भी पूजा-पाठ,अनुष्ठान के साथ समय-समय पर देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को मंत्रोच्चार द्वारा प्राणप्रतिष्ठित किया जाये तब व्यक्ति उस प्राणप्रतिष्ठित स्वरूप में समष्टि का विशिष्ट साकार रूप अनुभव कर अखण्ड पूजा-पाठ का आभास प्राप्त कर सके।
सत्यप्रतिष्ठा अर्थात जो चरमतत्व है वही सत्य है। सत्य का प्रतिष्ठित होने का भाव ही है कि मन,वचन,कर्म से हम जगत की असारता का त्याग कर सत्यस्वरूपा प्रतिष्ठित किये गये स्वरूप को ही समस्त इन्द्रियों को एकाग्रचित्त होकर ग्रहण करें और सत्य को छोड़ न कुछ देखेंगे, सुनेंगे,स्पर्श करेंगे या चिंतन करेंगे और पूरी तन्मयता उस सत्य के प्रति समर्पित होगी। सत्य स्वरूप है जिसे मूर्तिरूप में प्राणप्रतिष्ठित किया गया है। मूर्ति के स्वरूप में प्राणशक्ति के दर्शन का अर्थ परब्रम्ह के दर्शन करना, क्योंकि प्राण ही परब्रम्ह है। यह संसार और इसके संसारी हम लोग इसी परमब्रम्ह के अंश है, प्राणप्रतिष्ठित मूर्ति सागर है और हम उसकी लहरें। प्रतिमा में प्राणप्रतिष्ठित करना का अर्थ ही है कि प्रतिमा को यह शक्ति देना कि आप ही जगत की नियंता है, आप ही सब करने वाली है, हम प्राणीमात्र तो आपके खिलौने है, यहॉ व्यक्ति का अहंकार गिर जाता है और वह प्राणप्रतिष्ठित इस विग्रहमूर्ति में स्वयं परब्रम्ह का स्वरूप और भगवत्ता की आभा के प्रति नतमस्तक हो आत्मनिवेदन आनन्द और उल्लास से तृप्त होता है।
त्रेतायुग में राम के आराध्य शिव की मूर्तिरूप में पूजा एवं रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना का प्रमाण प्राप्त होता है इसी तरह त्रेतायुग में रावण सहित अन्य राजाओं के द्वारा सूर्यवंश के होने से सूर्य एवं चन्द्रवंश के होने से चन्द्र की पूजा का प्रमाण मिलता है। देवीय शक्ति को प्रसन्न करने के लिये मेघनाथ द्वारा अपनी कुलदेवी की पूजा के अलावा अन्यों द्वारा भी मूर्तिपूजन किया गया। द्वापर में भी शिव की मूर्तिपूजा के अनेक तथ्य है वही कृष्ण द्वारा गोवर्धनपूजा कर इन्द्रदेव को पूजने से वंचित किया गया है। कलयुग में मूर्ति पूजा का इतिहास तीन-साढे तीन हजार साल पुराना है जिसमें हमारी संस्कृति और मूर्तिकला की उत्कृष्ट शैली दक्षिण भारत सहित अनेक मंदिरों में देखी जा सकती है। अयोध्या में राम और मथुरा में कृष्ण सहित सम्पूर्ण भारत के मंदिरों में स्वरूपों की पूजा की चर्मोत्कृष्टतता थी जिसे सातवी सदी में मुस्लिम आतताईयों के आने के बाद भारतीय संस्कृति और धर्म को ध्वस्त कर मूर्तियों को तोड़ने और मंदिरों को ध्वस्त कर अरबों रूपयें के हीरे-जवाहारात और सोना को लूटा गया और विरोध करने वाले हिन्दूओं को कत्लकर दिया गया। जो मुस्लिम लुटेरों के सामने नतमस्तक हो गये उन्हें धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा।
भारत के कपाल पर छह-सात सो साल तक अनेक हिन्दु रियासतों, राज्यों पर मुस्लिम लुटेरों ने कब्जा किया एवं हिन्दुओं की अस्मिता एवं धर्म के साथ खिलवाड़ किया वहीं दो-ढाई सौ साल तक अंग्रेजों की गुलामी सही। भारत में मूर्तिपूजा गुजरे जमाने की बात होकर रह गयी फिर भी दक्षिण भारत सहित अनेक स्थानों पर मंदिरों के अस्तित्व को बचाकर लोग कुर्बानियॉ देते गये। इसलिये कृष्ण और राधा को पूजा में विलम्ब से स्थान मिला। इस बात के भी प्रमाण मिलते है कि उत्तर भारत के ग्रामीण अंचलों के घरों में गुर्जरी अर्थात गोपी की मूर्ति बनाने का प्रमुख धंधा था जिन्हें पूजने का प्रचलन दीपावली पर रहा है। कुम्भकार ही था जो इसके अलावा एक शताब्दी से इन मूर्तियों को लक्ष्मी,गणेश,दुर्गा आदि कई स्वरूपों में बनाकर व्यवसाय करता और लोग मूर्तियों को अपने घर लेजाकर तो कई सार्वजनिक स्थलों पर विराजित कर पूजते रहे जो अब भी जारी है।
विसर्जन एक गूढ़ दर्शन है। बिना विसर्जन के सृष्टि की कोई भी क्रिया संभव नहीं और विसर्जन के अभाव में सृष्टि में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पेड़-पौधे कार्बनडाईट आक्साईट गृहण कर आक्सीजन विसर्जित न करें तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। विसर्जन सृष्टि की एक निर्धारित प्रक्रिया है। पृथ्वी अपना अंश विसर्जित करती है तो पुष्प-अन्नादि उत्पन्न होता है। नदी बहाव के साथ जल विसर्जित करती है तो शुद्ध जल की प्राप्ति होती है। कुए का जल विसर्जित होता है तो जल के नये स्त्रोत पैदा होते है। जहॉ विसर्जन की गति अवरूद्ध होती है वहॉ विकृति पैदा हो जाती है। मनुष्य अन्नादि भोजन के बाद विसर्जित न करे तो कब्ज बैचेनी के साथ क्या हो सकता है, यह अनुभव करके सीखा जा सकता है। मानव समाज में प्रायः सभी लोग संग्रह, भोग तथा उपभोग में सतत कर्मशील रहकर विसर्जन करने अथवा त्याग करने के लिये सहज ही तत्पर नहीं होते, उसने अपील करनी होती है, प्रार्थना करनी होती है तब कहीं जाकर वे अपेक्षा पर ध्यान देते है लेकिन जब भी किसी को भोग के बाद विसर्जन की इच्छा होती है तब वे बिना किसी की सहमति-इच्छा के शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने दौड़ पड़ते है। शरीर के नैसर्गिक विसर्जन की प्रक्रिया सामान्य बात है जबकि यहॉ हम विसर्जन के जिस गूढ़तत्व को जिस दर्शन को व्यक्त करने जा रहे है वह जीवन का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक भाव है जहॉ आनन्द को जागृत कर वियोग के दुख और संयोग के सुख द्वारा मन को हृदयद्वार पर प्रतिष्ठित कर विसर्जन की प्रक्रिया में अनासक्ति की चेतना को प्राप्त किया जाता है।
देवी-देवता के प्राणप्रतिष्ठा के बाद आनन्दप्रतिष्ठा का महत्व है। आनन्द वास्तव में जगत की सृष्टि, स्थिति और लय के दोहन से प्राप्त होने वाला अमृतमय शब्द है। आनन्द शब्द परमब्रम्ह के दर्शन करने के बाद चित्त की जो दशा होती है उसकी अभिव्यक्ति से पैदा हुआ है इसलिये आनन्द को ब्रम्हानन्द का अंश माना है। हमारे अंतकरण और बहिकरण में जो विषयानन्द आनन्द के रूप में अनुभूत हुआ है वह समस्त आनन्द ब्रम्हानन्द की विभूति है जो सभी के मनों की कामना-वासना को अग्निकुण्ड में भस्मीभूत कर चिर आनन्द को प्रतिष्ठित करता है। हम मूर्ति में चैतन्य के एकीकरण द्वारा प्राणप्रतिष्ठा के पश्चात प्राणशक्ति से आनन्द प्राप्ति हेतु आनन्दप्रतिष्ठा को विस्मरण कर चुके है। हम उत्साह से भरे रहकर नवरात्रि पर दुर्गा-काली,नवदेवियों-शिवादि देवों के विभिन्न स्वरूपों को मंदिरों सहित सार्वजनिक स्थानों पर प्राणप्रतिष्ठित कर विराजित करते है तब प्राणप्रतिष्ठित उपास्यमूर्ति, या ईष्ट,देव को केवल मिट्टी की मूर्ति या कागज का चित्र मानकर उसकी भगवत्ता को जीवंत रूप देते है इसका चिंतन करना इसलिये आवश्यक हो गया क्योंकि आज जिस तरह गली-गली,घर-घर इन स्वरूपों को विराजित करने की अंधी परम्परा ने आस्था पर गहरी चोट करके सारी मान्य परम्पराओं को ध्वस्त किया है और स्थापना और विसर्जन के मुहुर्तो से हटकर निर्धारित समयावधि के पश्चात तक इन्हें विराजित कर धर्मान्धता में धर्म को विस्मृत किया जा चुका है।
मिट्टी की मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा के समय हमारा भाव उस स्वरूप को स्थापित करना भर नहीं होता बल्कि हम जितने दिन वे स्वरूप विराजित है उतने दिन उनकी पूजा-अर्चना और आराधना में लीन होते है। हम प्रसन्न होते है कि हम साधना-आराधना कर रहे है, जबकि अपने आराध्य के प्रति समर्पण की यह भक्ति कोई दिखावे या जतलावे का साक्ष्य नहीं मॉगती, आराधना स्वयं के कल्याण के लिये होती है। यहॉ यह भी विचारणीय है कि हम दुर्गा-काली, शिव आदि की स्थापना स्वयं प्रसन्नता से कर रहे है या भय के कारण, या इसलिये कि लोगों का आर्थिक सहयोग अधिक मिलता है और स्थापना पर खर्च न्यूनतम होने से लाभान्वित हो व्यवसायिक उद्देश्य या प्रलोभन पूरा होता हो। यदि ऐसा है तो यह उचित नहीं, होना तो चाहिये कि मातृशक्ति में भय नहीं करूणा के दर्शन कर आनन्दमय की प्राप्ति के लिये उनका आवाहन हो। जो भगवत्ता को नकारने या नास्तिक होने का दम भरता है वह भूल जाता है कि जगत की सत्ता, चैतन्य और आनन्द में विभूषित वहीं परम सत्ता को निन्दित करने वाला अपने आत्मीय स्वजन के मुख में आग लगाकर तिलांजलि देने को विवश होता है तब वह श्मशान में आन्दोलित हो भगवान के अनुसंधान के विचारों से भर जाता है।
हम साधक नहीं है फिर भी साधते है खुद को, हमारी पूजा-पाठ या आरित की कोई विधि तय नहीं होती है, हम तय विधि-आरति का पाठ कर साधक का अभिनय करने उतरते है। हमारे अपने कर्मकाण्डों ने ज्ञानकाण्डों ने हमें अपने आप में विवादित कर दिया है, यह हम भॅलीभॉति जानते समझते है पर प्रतिकार करने का साहस नहीं रखते है। हम पूजा का स्वाद नहीं जानते, हवन का स्वाद पता नहीं फिर भी समुद्र को अपनी हथेली में लेकर घूमने का अभिमान अवश्य रखते है। भॅले ही हमने वैदिक पद्धति को अपनाकर अपनी साधना-आराधना का धर्म निर्वहन किया है, तो भी हम ज्ञानी या कर्मयोगी नहीं हो गये है, बल्कि उस प्राणप्रतिष्ठित देवी-देव प्रतिमा को जो सम्पूर्ण प्रकृति में व्याप्त होते हुये आपके द्वारा मूर्ति में उनके मूलस्वरूप के साथ प्राणसंचारित की गयी, उस मूर्ति में उसका स्वरूप मौजूद है यह अनुभव से जिन्होंने भी आभासित किया है वह उस परमअनुभूति को व्यक्त नहीं कर सके। पॉच दशक पहले बाल्यावस्था में आरति के समय समवेत स्वरों में शीश चरणों में धरे मात विनय करते है, विजय हो देश की अरदास यही करते है, इस भाव्यानुभूति को सम्पर्ण सर्मपण के साथ करने के मेरे बालसुलभ मन की स्मृतियॉ ही मुझे जिज्ञासा से भरे हुये है जिसे आज व्यक्त करने हेतु मैं तत्पर हुआ हॅू और उस समय मैंने नर्मदा के पावन जल में शाम को शुरू होने से सुबह 4बजे तक देवी के विसर्जन का उत्सव देखा था तब सभी एक स्वरूप के विसर्जन के पश्चात अपने क्षैत्र की अन्य देवी-देव प्रतिमाओं के स्वरूप को पूरी श्रद्धा,जयकारों के साथ जल को अर्पित करके अर्थात विसर्जित करके ही नम ऑखों से लौटते थे, जैसे लगता था हम पीछे अपने बहुत ही आत्मीय स्वजन को छोड़कर आ रहे है। पूरे मोहल्ले में लोगों की ऑखों में उस दिन अश्रुधारा प्रवाहित होती थी और जिस स्थान पर देवी प्रतिमा प्राणप्रतिष्ठित की गयी थी उस स्थान से विदाई के बाद श्मशान की खामोशी में पूरा क्षैत्र डूब जाता था जिसका अंशमात्र भी आज यह वातावरण आभासित नहीं होता है।
मेरे मन में अनेक प्रश्न रहे है जिसमें यह विचार कौंधता है कि वैदिकयुग में कहीं भी शक्ति के स्वरूप या अन्य किसी देवी-देवता के स्वरूप को प्राणप्रतिष्ठित कर विराजित करने का कोई भी साक्ष्य किसी भी वेद पुराण या ग्रन्थ में नहीं है तब क्योंकर हम आज के परिवेश में गुरू-ईष्ट, भगवान के विभिन्न स्वरूपों सहित शक्ति स्वरूप को बिना उनका रहस्य समझे प्रत्येक वर्ष आने वाले पर्वो-त्यौहारों में कुछेक विशिष्ट दिन का मेहमान बनाकर मूर्तिरूप में प्राणप्रतिष्ठित कर विसर्जन की चेष्टायें करते है? यह भी तार्किक प्रश्न है कि जीवन में शक्ति सर्वोपरि है और शक्ति के बिना ऑखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ-पैर चल नहीं सकते, मन चिंतन नहीं कर सकता है और प्राण जीवित नहीं रह सकते है। शक्ति के अभाव में मॉ-बाप, बहिन-भाई, सगे-सम्बन्धियों का तथा हमारा अस्तित्व शून्य हो जाता है इसीलिये शक्ति को सच्चिदानंद परमपिता माना है और वे परमपिता ही हमें जीवित रखने में, ज्ञान,आनन्द,सुख-शान्ति,सौन्दर्य और जगत की अहेतुक कृपा का दान देने में निमग्न है, इसलिये हम उस शक्तिस्वरूप परमपिता और प्रकृतिस्वरूपा शक्ति के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को अभिव्यक्त करें।
शक्तिप्रकाशस्वरूपा है जिसे प्रकाशपुंज भी कहा गया है,पकाशस्वरूपा इसलिये क्योंकि वह स्वयंप्रकाश है, उन्हें प्रकाशित नहीं होना होता और न ही प्रकाश करना पड़ता है स्वयं श्रीमदभागवत गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन के समक्ष इसका रहस्य प्रतिपादित किया है और परमात्मा के परम प्रकाश के दर्शन के लिये हमारी दृष्टि का परदा जगत के दृश्यमान के लिये बतलाकर एक अलौकिक दिव्य दृष्टि प्रदान कर स्वयं प्रकाशवान के दर्शन कराये है।
मैंने पूर्व में शक्ति के सम्बन्ध में जिस प्रकार शरीर, शरीर के अंग, परिवार-कुटुम्ब आदि का उदाहरण दिया उसी में दूसरा वृहदरूप शक्तिरूप पूजित करने से पहले उसके विस्तार पर भी चिंतन जरूरी है। शक्ति सभी चाहते है, दुनिया के हर देश चाहते है कि वे शक्तिशाली हो जाये। जीवनधारण के लिये शक्ति की आवश्यकता सभी को है वैसे ही ज्ञानार्जन, भगवतप्राप्ति आदि में शक्ति की उपासना मूल में है इसलिये सभी और शक्ति प्राप्ति पर बल दिया गया है। ब्रम्हा हो, शिव हो या विष्णु, सभी विभिन्न प्रयोजनों के लिये शक्ति का आवाहन कर शक्ति प्राप्ति उपरांत सृष्टि के कार्य संपादित करते है। काली, दुर्गा, कात्यायिनी, योगमाया आदि सभी शक्तिस्वरूपा के प्राप्ति का मार्ग तंत्रविद्या,मंत्रविद्या, श्रीविद्या, कालीविद्या जैसे कर्मकाण्डों द्वारा संभव है इसलिये शक्तिप्राप्ति की दौड़ में आज का हर व्यक्ति इन विद्याओं का अनुकरण-अनुसरण कर स्वयं को शक्तिशाली करना चाहता है। पृथक-पृथक अपने मनोयोग से अपने-अपने संसार में मनुष्य कार्यरत है और जैसे सभी जीवों,प्राणियों, वनस्पतियों आदि का जन्मदाता परमात्मा है, तो उसी तरह मनुष्य भी उसी भगवान की संतान विभूषित है।
शक्ति की आराधना में करोड़ों लोग रत रहते है लेकिन मुश्किल से आधा-एक प्रतिशत भक्त ही मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा के साथ सत्यप्रतिष्ठा एवं आनन्दप्रतिष्ठा को अपनी कर्मेन्द्रियों से विजयीहुआ पा पाता है शेष भीड़ के अंग बने हुये भक्तों की कतार में आधे-अधूरे मन से नियम पालना में स्वयं को इस आराधना में त्रिशंकु की भॉति मझदार में होते है। कड़वा सच तो यह है कि विषयभोगों में लिप्त ये भक्त न तो भक्ति से भगवान को तृप्त कर पाते है और न ही स्वयं की तृप्ति पा पाते है और उनकी समस्त वृत्तियॉ कल्याण मार्ग पर होते हुये साधना के अभाव में उन्हें उनके साध्य की प्राप्ति से वंचित रखती है। ऐसे भक्त एक तोते की तरह रटना सीख लेते है, लेकिन रटने से ईष्ट की कृपा अप्राप्त रहती है,जबकि अगर ये मिट्टी की मूर्तिस्वरूप के जीवंतता से अपने मन का उपचार कराकर समर्पित हो जाये तो इनके यही प्रयास उन्हें अर्हनिश आर्शीवाद और मूर्ति में विराजमान ईष्टतत्व इनकी इन्द्रियों में सर्वत्र सुखानुभव का संचार कर इनके अंतकरण में आनन्दोत्सव की त्रिवेणी के मंगलप्रकाश का स्नान करा दे,जिससे ये अभी तक अनहाये हुये है।
शक्ति उपासना का पर्व चैत्र एवं शारदीय नवरात्रि पर परम्परागत देवीयों के मिट्टी के श्रीविग्रह को प्राणप्रतिष्ठित करने के स्थलों-मंदिरों के अलावा अब जगह-जगह विराजित कर पूजा करने का प्रचलन शुरू हुआ है ठीक वैसे ही गणेशोत्सव पर गणेश एवं अन्य स्वरूपों को गली-गली-चौक-चौक विराजित करने की होड़ लगी है। यह होड़ भक्तों की नहीं प्रतिस्पर्धा करने वाले नयनहीनों की है जो महत्वपूर्ण चौराहों-मार्गो पर भूमि कब्जाने,राजनीति की दूकान चलाने, चंदा कर जनता को तंग करने वालों की है जिन्हें मूर्ति विराजित करते समय न तो प्राणप्रतिष्ठा का भान होता है, न वे सत्यप्रतिष्ठा एवं आनन्दप्रतिष्ठा के राजयोग को समझते है। कानून व्यवस्था को चौपट कर धर्मध्वजा थामे ये न तो मुहुर्त में प्राणप्रतिष्ठा कराने और मुहुर्त में विसर्जन के भाव को समझे निश्चित समयावधि के पश्चात कई दिनों तक प्राणप्रतिष्ठित ईष्ट को रोककर उनकी वैदिक रीति से सेवा-सुश्रवा कर पाते है न ही समन्वय स्थापन के भाव को कायम रखकर अपनी मनमानी करके विसर्जन के स्वरूप को विकृति प्रदान कर चुके है जिससे प्राणप्रतिष्ठित देवों का अभिश्राप हमारे कल्याण की जगह हमें दिनोंदिन अवन्नति की ओर अग्रसर किये हुये है।
सृष्टि में सभी का समय निर्धारित है। जीवन का समय हो या मृत्यु का, यह पूर्व ही तय किया जा चुका है। जन्म को स्वीकारना उत्सव है तो विसर्जन को महाउत्सव की भॉति मनाकर हम जीवन का सम्मान करते है। मिट्टी की मूरत को जब हम प्राणप्रतिष्ठित से संजीवितकर उनके प्रति समर्पितभाव से स्नानादि,पूजा-पाठ,भोग्यादि के साथ उन्हें सुलाने एवं जगाने का पुण्यकर्म करते है तब उस स्वरूप के प्रति हमारा बाहरी ज्ञान ही नहीं अपितु मानसिक पूजा के साथ हमारी देह का समपर्ण हमें एक आनन्द से भर देता है। यही आनन्द और प्रत्येक तत्व की अनुभूति प्राणप्रतिष्ठित प्रतिमा में विराजमान होने पर एक निश्चित समय,मुर्हुत पर ईष्टप्रतिमा को उनके मूलस्थान पर भेजने के आशय से उन्हें मन की ज्ञानगंगा में विसर्जन के भाव के साथ पुनः बुलाने पर आने की प्रार्थना लिये किसी पावन नदी, तालाब आदि के शुद्ध जल में विसर्जित करते है। भक्त के मन की त्रिवेणी में भगवान की सूक्ष्म प्रतिमा का विसर्जन भक्त के लिये कल्याणकारी होता है और भक्त अपने अंतस में विसर्जित इस अदृश्य हुई सूक्ष्म प्रतिमा को तन्मयता के साथ अपने हृदयसागर में समा लेता है, यही भाव विसर्जन का है। जब भक्त के हृदय में ज्ञान के प्रकाश के रूप में प्रतिमा का सूक्ष्मतम स्वरूप प्रकाशित हो जाये तो बाहर जो शेष रहेगा वह प्रतिमा का स्थूलरूप होगा जिसे जपादि करते हुये प्रकृतिस्वरूपा शक्तिपुंज शक्तिविग्रह प्रतिमा को बाहरी जगत में जल को अर्पितकर विसर्जित किया जाता है, यही विश्वरूपा,समृष्टिभूता परमात्मा की अनुकम्पा का मार्ग है जो सहज ही हमें उपलब्ध होता है। विसर्जनकर्ता ममत्व का विसर्जन करके त्याग करता है। त्याग उसकी आसक्तियों का होता है। स्वेच्छा से विवेकपूर्ण विसर्जन ही आनन्ददायक होता है, इसलिये व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्व से मुक्त होकर विसर्जन करता है तो वह आनन्द की चर्मोत्कृष्टता होती है।
आत्माराम यादव पीव वरिष्ठ पत्रकार,
श्रीजगन्नथधाम काली मंदिर के पीछे, ग्वालटोली
नर्मदापुरम मध्यप्रदेश मोबाइल 9993376616